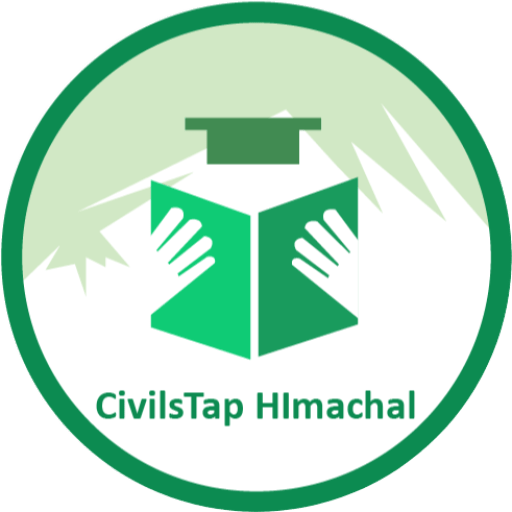- Phone :+917814622609
- Email :civilstaphimachal@gmail.com
- Student Dashboard
Allied MAINS EXAM 2025
Hindi Paper
1. निम्नलिखित अंग्रेजी अवतरण का हिंदी 30
Hindu philosophy beautifully compares a judge with a flower which would never wither and remains ever fresh. An anecdote very appropriately explains this concept- A religious discussion was to take place between Adi Shankaracharya and Mandan Mishra. Sharda or Saraswati was judge. Both were offered similar asanas to sit on. Having plucked fresh flowers. Sharda strung two identical garlands. She put them round the necks of the two scholars and said , “During the discussion, the garlands will decide the winner and the loser. The wearer of the garland whose flowers fade first will be considered to have lost.” Sharda maintained that, “He who possessed intellectual clarity, power of thinking and self-confidence will be calm and peaceful. His voice will be like the cool spring. Therefore, the flowers will remain fresh for a longer time. On the other hand, one who does not have a clear intellect or a strong sense of logic or whose self-confidence staggers, will be frustrated. His voice will become harsh, the circulation of blood in his veins will become rapid and his breath will become hot. Hence the flowers around his neck will whither sooner.” The fragrance and freshness of flowers become a part of the personality of a judge if what he thinks and what he does are all based on such values as are the canons of judicial ethics.
हिंदू दर्शन खूबसूरती से एक न्यायाधीश की तुलना एक फूल से करता है जो कभी मुरझाता नहीं है और हमेशा ताजा रहता है। एक किस्सा इस अवधारणा को बहुत उपयुक्त रूप से समझाता है- आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच एक धार्मिक चर्चा होनी थी। शारदा या सरस्वती न्यायाधीश थे। दोनों को बैठने के लिए एक जैसे आसन दिए गए। ताजे फूल तोड़कर, शारदा ने दो समान मालाएं पकड़ी थीं। उसने उन्हें दोनों विद्वानों के गले में डाल दिया और कहा, “चर्चा के दौरान, माला विजेता और हारने वाले का फैसला करेगी। जिस माला के फूल पहले मुरझाते हैं, उसे पराजित माना जाएगा। शारदा ने कहा कि, “जिसके पास बौद्धिक स्पष्टता, सोचने की शक्ति और आत्मविश्वास है, वह शांत और शांतिपूर्ण रहेगा। उसकी आवाज शांत वसंत की तरह होगी। इसलिए, फूल लंबे समय तक ताजा रहेंगे। दूसरी ओर, जिसके पास स्पष्ट बुद्धि या तर्क की मजबूत भावना नहीं है या जिसका आत्मविश्वास डगमगाता है, वह निराश होगा। उसकी आवाज कठोर हो जाएगी, उसकी नसों में रक्त का संचार तेज हो जाएगा और उसकी सांस गर्म हो जाएगी। इसलिए उसके गले में फूल जल्द ही फड़फड़ाएंगे। फूलों की सुगंध और ताजगी एक न्यायाधीश के व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन जाती है यदि वह जो सोचता है और जो करता है वह सभी ऐसे मूल्यों पर आधारित है जैसे न्यायिक नैतिकता के सिद्धांत हैं।
2. निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या कीजिए: 20
मनुष्य लोकबद्ध प्राणी है, इससे वह अपने को उनके कर्मों के गुण-दोष का भी भागी समझता है जिनसे उसका सम्बन्ध होता है, जिनके साथ वह देखा जाता है। पुत्र की अयोग्यता और दुराचार, भाई के दुर्गुण और असभ्य व्यवहार आदि का ध्यान करके भी दस आदमियों के सामने सिर नीचा होता है। यदि हमारा साथी हमारे सामने किसी तीसरे आदमी – से बातचीत करने में भारी मूर्खता का प्रमाण देता है भद्दी और ग्राम्य भाषा का प्रयोग करता है, तो हमें भी लज्जा आती है। जिसे लोग कुमार्गी जानते हैं, उसके साथ यदि हम कभी देव मंदिर के मार्ग पर भी देखे जाते हैं तो सिर झुका लेते हैं या बगलें झाँकते हैं। बात यह है कि जिसके साथ हम देखे जाते हैं, उसका हमारा कितनी बातों में कहाँ तक साथ है, दूसरों को इसके अनुमान की पूरी स्वच्छंदता रहती है, उनकी कल्पना की कोई सीमा हम तत्काल बाँध नहीं सकते।
गद्यांश की व्याख्या:
इस गद्यांश में यह बताया गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में उसका अस्तित्व दूसरों से जुड़ा हुआ है। वह केवल अपने कर्मों के आधार पर ही नहीं, बल्कि अपने संबंधियों, मित्रों और परिचित के कर्मों के गुण-दोष का भी भागी समझा जाता है। इस कारण, यदि उसके निकट संबंधी या साथी अनुचित आचरण करते हैं, तो वह स्वयं को लज्जित अनुभव करता है।
उदाहरण के रूप में, यदि किसी व्यक्ति का पुत्र या भाई अयोग्य, दुर्व्यवहारी या असभ्य होता है, तो समाज में उस व्यक्ति की भी प्रतिष्ठा प्रभावित होती है। इसी प्रकार, यदि कोई मित्र किसी से बातचीत करते समय मूर्खता या भद्दी भाषा का प्रदर्शन करता है, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है, और हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। लेखक इस संदर्भ में यह भी बताते हैं कि कुछ लोग अपने पालतू कुत्तों की बदतमीजी पर भी शर्मिंदा हो जाते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य का सामाजिक अस्तित्व उसके चारों ओर के वातावरण से जुड़ा हुआ है।
गद्यांश में यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जिसे समाज कुमार्गी (दुश्चरित्र) मानता है, हमारे साथ मंदिर के रास्ते पर भी देखा जाता है, तो लोग हमें भी संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं। इसका कारण यह है कि समाज के पास यह स्वतंत्रता होती है कि वह हमारे संबंधों और मेल-जोल को देखकर हमारे चरित्र का आकलन करे। लोगों की कल्पना की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए वे हमारे वास्तविक संबंधों की गहराई का अनुमान नहीं लगाते, बल्कि बाहरी दिखावे के आधार पर धारणा बना लेते हैं।
निष्कर्ष:
इस गद्यांश के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि समाज में मनुष्य की प्रतिष्ठा केवल उसके व्यक्तिगत कार्यों से ही नहीं, बल्कि उसके संबंधों और संगति से भी प्रभावित होती है। इसलिए हमें अपने आचरण के साथ-साथ अपने संपर्कों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लोग हमें हमारे साथियों और संबंधों के आधार पर भी परखते हैं।
3. निम्नलिखित काव्यांश की व्याख्या कीजिए: 15
आसमान की ओढ़नी ओढ़े
धानी पहने फसल घँघरिया
राधा बन कर धरती नाची,
नाचे हँसमुख कृषक सँवरिया ।
माती थाप हवा की पड़ती,
पेड़ों की बज रही ढुलकिया,
जी-भर फाग पखेरू गाते
ढरकी रस की राग-गगरिया
मैंने ऐसा दृश्य निहारा
मेरी रही न मुझे खबरिया-
खेतों के नर्तन उत्सव में
भूला तन-मन गेह डगरिया ।
पंक्तियों की व्याख्या:
इन काव्य-पंक्तियों में कवि ने प्रकृति और कृषि-परिवेश का एक सुंदर और जीवंत चित्रण किया है। इस कविता में धरती को नृत्य करती हुई राधा के रूप में प्रस्तुत किया गया है और कृषक (किसान) को कृष्ण स्वरूप में दिखाया गया है। पूरी कविता में उत्सव, आनंद और प्रकृति की सुन्दरता झलकती है।
पहली चार पंक्तियाँ:
“आसमान की ओढ़नी ओढ़े,
धानी पहने फसल घँघरिया,
राधा बन कर धरती नाची,
नाचे हँसमुख कृषक सँवरिया।”
यहाँ कवि ने प्रकृति की सुंदरता का अद्भुत चित्र खींचा है। आसमान को ओढ़नी (दुपट्टा) के रूप में दिखाया गया है, जो धरती पर फैला हुआ है। हरी-भरी फसलें ‘धानी रंग’ (हरा रंग) की साड़ी पहने हुए प्रतीत होती हैं। धरती को नृत्यरत राधा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो अपनी हरियाली से आनंदित हो रही है। इसी प्रकार, कृषक (किसान) को कृष्ण रूप में दिखाया गया है, जो प्रसन्न होकर नृत्य कर रहा है। यह दृश्य बताता है कि धरती और किसान दोनों फसल के पकने से आनंदित हैं।
अगली चार पंक्तियाँ:
“माती थाप हवा की पड़ती,
पेड़ों की बज रही ढुलकिया,
जी-भर फाग पखेरू गाते,
ढरकी रस की राग-गगरिया।”
यहाँ कवि ने प्राकृतिक वातावरण को और अधिक सजीव बनाया है। हवा की थपकियों को ताल व थाप की तरह बताया गया है, जिससे मानो धरती झूम रही हो। पेड़ हिलते-डुलते हुए मधुर संगीत उत्पन्न कर रहे हैं। पक्षी भी फागुनी गीत गा रहे हैं, मानो वे भी इस आनंदोत्सव का हिस्सा बन गए हों। रस से भरी हुई गगरी (मटकी) से जैसे मधुर संगीत झर रहा हो, वैसे ही यह प्राकृतिक दृश्य मधुरता से भरपूर है।
अंतिम चार पंक्तियाँ:
“मैंने ऐसा दृश्य निहारा,
मेरी रही न मुझे खबरिया-
खेतों के नर्तन उत्सव में,
भूला तन-मन गेह डगरिया।”
कवि कहता है कि जब उसने यह अद्भुत दृश्य देखा, तो वह इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसे अपनी सुध-बुध ही नहीं रही। खेतों में हो रहे इस उत्सव में वह पूरी तरह खो गया और अपने घर-परिवार, राह और अपनी चेतना तक को भूल गया। इस पंक्ति में प्रकृति और मनुष्य के गहरे संबंध को दिखाया गया है, जहाँ किसान अपनी मेहनत और धरती की उर्वरता से इतने प्रसन्न होते हैं कि उनके लिए यही सबसे बड़ा उत्सव बन जाता है।
निष्कर्ष:
इस कविता में प्रकृति और कृषि-समाज के सौंदर्य और उल्लास का अनुपम चित्रण है। धरती और किसान के बीच का आत्मीय संबंध इस प्रकार दर्शाया गया है कि मानो दोनों एक होकर नृत्य कर रहे हों। यह कविता प्रकृति, खेती, और फसल की समृद्धि के प्रति किसान की प्रसन्नता और समर्पण को दर्शाती है।
4. निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 1000 (एक हज़ार) शब्दों में निबंध लिखिए: 40
(i) इज़राइल – ईरान तनाव का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
इज़राइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का भारतीय अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभावों पर चर्चा करते हुए, हमने पहले ही कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, महंगाई दर में वृद्धि, रुपये पर दबाव, व्यापार घाटा, शेयर बाजार में अस्थिरता, सोने की कीमतों में उछाल, और व्यापार एवं निर्यात पर असर जैसे बिंदुओं पर चर्चा की है। अब, हम इस संदर्भ में कुछ अतिरिक्त आंकड़े और विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे:
- ऊर्जा आपूर्ति और मूल्य निर्धारण की गतिशीलता
- ईरान का तेल उत्पादन: ईरान प्रतिदिन लगभग 3.2 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन करता है, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग 3% है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद, चीन में बढ़ती मांग के कारण ईरान के तेल निर्यात में वृद्धि देखी गई है।
- ओपेक की अतिरिक्त क्षमता: ओपेक+ के पास अतिरिक्त तेल उत्पादन क्षमता है, जिसमें सऊदी अरब प्रतिदिन 3 मिलियन बैरल और यूएई लगभग 1.4 मिलियन बैरल उत्पादन बढ़ा सकते हैं। यह क्षमता संभावित ईरानी आपूर्ति व्यवधानों के विरुद्ध एक बफर प्रदान करती है।
- व्यापार मार्गों में व्यवधान
- लाल सागर और स्वेज नहर मार्ग: भारत के यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और पश्चिम एशिया के साथ व्यापार के लिए लाल सागर और स्वेज नहर मार्ग महत्वपूर्ण हैं, जिनसे प्रतिवर्ष 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य के माल का आवागमन होता है। संघर्ष के कारण इन मार्गों में व्यवधान का जोखिम बढ़ सकता है।
- निर्यात पर आर्थिक प्रभाव
- निर्यात में गिरावट: अगस्त 2024 में, लाल सागर में संकट के कारण भारत के निर्यात में 9% की गिरावट देखी गई, विशेष रूप से पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात में 38% की भारी गिरावट आई।
- बढ़ती शिपिंग लागत
- शिपिंग लागत में वृद्धि: संघर्ष के कारण शिपिंग मार्ग लंबे हो जाने से लागत में 15-20% की वृद्धि हुई है, जिससे भारतीय निर्यातकों के लाभ मार्जिन पर असर पड़ा है, विशेष रूप से निम्न-स्तरीय इंजीनियरिंग उत्पादों, वस्त्रों और परिधानों के निर्यातकों के लिए।
- भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC)
- IMEC पर प्रभाव: भारत की जी-20 अध्यक्षता के दौरान प्रस्तावित IMEC का उद्देश्य स्वेज नहर पर निर्भरता को कम करना है। हालांकि, जारी संघर्ष से इस गलियारे की प्रगति और व्यवहार्यता को खतरा है, जिससे भारत और उसके साझेदारों के बीच द्विपक्षीय व्यापार प्रभावित हो सकता है।
- भारतीय बाजारों पर प्रभाव
- शेयर बाजार में गिरावट: तेल की कीमतों में वृद्धि से निवेशकों का ध्यान भारतीय इक्विटी से हटकर बॉन्ड या सोने जैसी सुरक्षित परिसंपत्तियों की ओर जा सकता है। इससे भारतीय शेयर बाजार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जैसा कि सेंसेक्स और निफ्टी जैसे प्रमुख सूचकांकों में गिरावट से देखा गया है।
- सुरक्षित परिसंपत्ति के रूप में सोना
- सोने की कीमतों में वृद्धि: भू-राजनीतिक तनाव और निवेश रणनीतियों में बदलाव के कारण सोने की कीमतें नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई हैं, क्योंकि अनिश्चितता के समय में निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की ओर आकर्षित होते हैं।
निष्कर्ष
इज़राइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुआयामी प्रभाव पड़ सकता है, जिसमें ऊर्जा आपूर्ति, व्यापार मार्ग, निर्यात, शिपिंग लागत, आर्थिक गलियारे, वित्तीय बाजार, और सुरक्षित निवेश शामिल हैं। सरकार को इन संभावित चुनौतियों का सामना करने के लिए रणनीतिक उपाय करने होंगे, जिससे अर्थव्यवस्था की स्थिरता और विकास को बनाए रखा जा सके।
यदि आप इस विषय पर और अधिक विशिष्ट जानकारी या विश्लेषण चाहते हैं, तो कृपया बताएं।
(ii) प्रसंस्कृत (processed) खाद्य का भारतीय पारिवारिक संस्कृति पर प्रभाव
भारत में पारंपरिक भोजन संस्कृति घर के बने ताजे और पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों पर आधारित रही है। लेकिन हाल के दशकों में, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की बढ़ती लोकप्रियता ने भारतीय परिवारों की खान-पान की आदतों, स्वास्थ्य, और पारिवारिक संस्कृति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है।
- पारिवारिक भोजन संस्कृति में बदलाव
घर पर खाना पकाने की परंपरा में गिरावट
- पहले भारतीय परिवारों में महिलाएं और बुजुर्ग घर के भोजन को प्राथमिकता देते थे, लेकिन अब तैयार-खाने वाले (ready-to-eat) और इंस्टेंट फूड्स का चलन बढ़ गया है।
- संयुक्त परिवार के एकल परिवार के बढ़ने से पारंपरिक व्यंजन कम बन रहे हैं, और रेडी-टू-ईट भोजन, इंस्टेंट नूडल्स, पैकेज्ड स्नैक्स का उपयोग बढ़ा है।
सामूहिक भोजन की परंपरा पर असर
- पहले भारतीय परिवार एक साथ बैठकर भोजन करते थे, जिससे पारिवारिक संवाद और बंधन मजबूत होते थे।
- अब फास्ट फूड और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की उपलब्धता के कारण अलग-अलग समय पर और जल्दी-जल्दी भोजन करने की प्रवृत्ति बढ़ी है।
- स्वास्थ्य पर प्रभाव
जंक फूड और मोटापा बढ़ने की समस्या
- प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में उच्च मात्रा में नमक, चीनी और ट्रांस फैट होता है, जिससे मोटापा, डायबिटीज और हृदय रोग जैसी बीमारियाँ बढ़ रही हैं।
- भारत में बच्चों में मोटापा 2000 से 2020 के बीच दोगुना हो गया। WHO के अनुसार, भारत में 14.4 मिलियन मोटे बच्चे हैं, जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है।
पारंपरिक आहार से दूरी
- प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के बढ़ते उपयोग से पारंपरिक, घर के बने पोषक खाद्य पदार्थों की उपेक्षा हो रही है, जिससे शरीर को आवश्यक पोषण नहीं मिल पाता।
- आयुर्वेद में संतुलित और ताजे भोजन को स्वास्थ्य के लिए आवश्यक माना गया है, लेकिन आधुनिक जीवनशैली में यह आदत कमजोर पड़ती जा रही है।
- सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव
फास्ट फूड संस्कृति का बढ़ना
- मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, पिज्जा हट जैसी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के भारत में विस्तार से फास्ट फूड संस्कृति लोकप्रिय हुई है।
- जन्मदिन, शादी, और अन्य सामाजिक आयोजनों में अब पारंपरिक व्यंजनों के स्थान पर पिज्जा, बर्गर, पैकेज्ड स्नैक्स अधिक पसंद किए जाते हैं।
स्थानीय व्यंजनों पर प्रभाव
- प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की अधिकता से भारत की समृद्ध क्षेत्रीय भोजन परंपराएँ प्रभावित हो रही हैं।
- कई पारंपरिक व्यंजन, जैसे कि बाजरे की रोटी, सत्तू, घर का बना अचार आदि, अब कम प्रचलित हो रहे हैं।
- पर्यावरण और आर्थिक प्रभाव
प्लास्टिक और पैकेजिंग कचरा बढ़ना
- प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग से प्लास्टिक कचरा बढ़ रहा है, जिससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- भारत में हर साल 3.5 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें से अधिकांश फूड पैकेजिंग से आता है।
स्थानीय उत्पादों की मांग में कमी
- पारंपरिक भारतीय कृषि आधारित खाद्य पदार्थों की मांग कम हो रही है, जिससे स्थानीय किसानों और छोटे व्यापारियों को नुकसान हो रहा है।
- प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग बड़े कॉरपोरेट्स द्वारा नियंत्रित होने के कारण छोटे खाद्य उत्पादकों पर दबाव बढ़ रहा है।
निष्कर्ष
प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का भारतीय पारिवारिक संस्कृति पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। यह सुविधा और त्वरित उपलब्धता के कारण लोकप्रिय हो रहे हैं, लेकिन इससे स्वास्थ्य, पारिवारिक संबंधों और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है। हमें पारंपरिक आहार और स्वास्थ्यप्रद भोजन की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता बढ़ाने और संतुलित खानपान अपनाने की आवश्यकता है।
(समाधान)
- घरेलू भोजन को प्राथमिकता दें – सप्ताह में कम से कम 5 दिन घर का बना खाना खाएं।
प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सीमित सेवन करें – अत्यधिक चीनी, नमक और वसा वाले खाद्य पदार्थों से बचें।
स्थानीय और पारंपरिक भोजन को अपनाएं – बाजरा, दाल, छाछ, और मौसमी सब्जियों को आहार में शामिल करें। - बच्चों को हेल्दी फूड के प्रति जागरूक करें – उन्हें घर पर बने स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन खाने की आदत डालें।
प्लास्टिक पैकेजिंग को कम करें – ज्यादा से ज्यादा ताजे और खुले में मिलने वाले खाद्य पदार्थों को खरीदें।
(iii) एक राष्ट्र एक चुनाव: अवधारणा एवं व्यावहारिक पक्ष
“एक राष्ट्र, एक चुनाव” (One Nation, One Election) का विचार भारत में एक ही समय पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराने से संबंधित है। यह प्रणाली चुनाव प्रक्रिया को सरल और किफायती बनाने के उद्देश्य से प्रस्तावित की गई है।
- अवधारणा (Concept)
“एक राष्ट्र, एक चुनाव” का अर्थ है कि देशभर में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं, ताकि बार-बार होने वाले चुनावों से बचा जा सके। यह प्रस्ताव भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83(2) और 172(1) से संबंधित है, जो लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित करता है।
इतिहास में झलक
- 1952, 1957, 1962 और 1967 में भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे।
- 1968-69 में कुछ राज्यों में सरकारें अस्थिर होने के कारण यह व्यवस्था टूट गई।
- 1983 में चुनाव आयोग ने इसे फिर से लागू करने की सिफारिश की थी।
- 1999 में विधि आयोग ने भी “समान चुनाव चक्र” की वकालत की थी।
- 2018 में विधि आयोग की रिपोर्ट ने इसे लागू करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता बताई।
व्यावहारिक पक्ष (Practical Aspects)
(A) संभावित लाभ
चुनाव लागत में कमी
- बार-बार चुनाव कराने में हजारों करोड़ रुपये खर्च होते हैं।
- 2019 लोकसभा चुनाव में ₹60,000 करोड़ से अधिक खर्च हुआ।
- यदि सभी चुनाव एक साथ हों, तो सरकारी और राजनीतिक दलों का खर्च कम होगा।
शासन की स्थिरता और विकास कार्यों में तेजी
- चुनावों के कारण आचार संहिता लागू होती है, जिससे विकास कार्य रुक जाते हैं।
- बार-बार चुनाव होने से सरकार और प्रशासन नीति-निर्माण पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाते।
- सभी चुनाव एक साथ होने से सरकारें पूर्ण कार्यकाल तक काम कर पाएंगी।
चुनावी बोझ और आचार संहिता का प्रभाव कम होगा
- हर कुछ महीने में किसी न किसी राज्य में चुनाव होते हैं, जिससे प्रशासन, सुरक्षा बलों और जनता पर बोझ बढ़ता है।
- एक साथ चुनाव कराने से बार-बार लागू होने वाली आदर्श आचार संहिता (MCC) का प्रभाव कम होगा और योजनाएँ निर्बाध रूप से लागू हो सकेंगी।
मतदाताओं की भागीदारी बढ़ सकती है
- अलग-अलग समय पर चुनाव होने से लोगों में मतदान के प्रति रुचि कम होती है।
- एक साथ चुनाव होने से मतदाता अधिक जागरूक और उत्साहित होंगे।
(B) संभावित चुनौतियाँ
संवैधानिक और कानूनी जटिलताएँ
- लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अलग-अलग होता है।
- संविधान में अनुच्छेद 83(2) और 172(1) के तहत 5 साल की अवधि का प्रावधान है, लेकिन सरकारें अस्थिर होने पर कार्यकाल पूरा नहीं कर पातीं।
- इसके लिए संविधान में संशोधन (अनुच्छेद 324, 83, 172, 356) करना आवश्यक होगा।
संसदीय प्रणाली पर प्रभाव
- अगर किसी सरकार को बीच में ही भंग करना पड़े, तो क्या पूरे देश में फिर से चुनाव कराए जाएंगे?
- राष्ट्रपति शासन का उपयोग बढ़ सकता है, जिससे संघवाद प्रभावित हो सकता है।
विपक्षी दलों की असहमति
- कई क्षेत्रीय दल मानते हैं कि “एक राष्ट्र, एक चुनाव” से राष्ट्रीय दलों को फायदा होगा और क्षेत्रीय दलों का प्रभाव कम होगा।
- इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
मतदान प्रक्रिया और ईवीएम की जरूरत
- पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कई लाख ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की जरूरत होगी।
- वर्तमान में भारत के पास इतनी बड़ी संख्या में ईवीएम उपलब्ध नहीं हैं।
संभावित समाधान
आंशिक रूप से लागू करना
- सभी राज्यों को दो समूहों में विभाजित किया जाए और प्रत्येक समूह में 2.5 साल के अंतराल पर चुनाव कराए जाएं।
विश्वास मत और राष्ट्रपति शासन के विकल्प
- यदि किसी राज्य की सरकार भंग होती है, तो राष्ट्रपति शासन लागू करने के बजाय अंतरिम सरकार बनाई जाए ताकि पूरा चुनाव चक्र प्रभावित न हो।
संसदीय सहमति और राजनीतिक संवाद
- राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनानी होगी ताकि चुनाव सुधार लागू किए जा सकें।
- निष्कर्ष (Conclusion)
“एक राष्ट्र, एक चुनाव” एक महत्वाकांक्षी विचार है जो चुनावी खर्च को कम करने, नीति-निर्माण को मजबूत करने और शासन की स्थिरता बनाए रखने में मदद कर सकता है। लेकिन इसे लागू करने के लिए संविधान संशोधन, राजनीतिक सहमति और प्रशासनिक सुधारों की जरूरत होगी। यदि इन चुनौतियों का समाधान किया जाता है, तो यह लोकतंत्र को और अधिक प्रभावी बना सकता है।
(iv) इक्कीसवीं सदी में साहित्य और कला
इक्कीसवीं सदी में साहित्य और कला
इक्कीसवीं सदी में साहित्य और कला ने नए सामाजिक, तकनीकी और सांस्कृतिक परिवर्तनों के साथ कदमताल किया है। वैश्वीकरण, डिजिटल क्रांति, और नई विचारधाराओं के प्रभाव से साहित्य और कला के स्वरूप में बड़ा बदलाव आया है।
इक्कीसवीं सदी में साहित्य
(A) साहित्य की प्रवृत्तियाँ
डिजिटल युग और ऑनलाइन साहित्य
- ई-बुक्स, ऑडियोबुक्स और किंडल जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों ने साहित्य को व्यापक रूप से सुलभ बना दिया है।
- ब्लॉग, ऑनलाइन मैगज़ीन और सोशल मीडिया ने नए लेखकों को पहचान दिलाने में मदद की है।
- फ्लैश फिक्शन और माइक्रो-लिटरेचर (150-300 शब्दों की कहानियाँ) लोकप्रिय हुई हैं।
यथार्थ वाद और समकालीन विषय
- आधुनिक साहित्य में आर्थिक असमानता, जलवायु परिवर्तन, नारीवाद, जातिवाद, और मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषय अधिक चर्चा में हैं।
- डिस्टोपियन और साइंस फिक्शन साहित्य (जैसे “ब्लैक मिरर” जैसी कहानियाँ) भविष्य की चिंताओं को व्यक्त कर रहा है।
अनुवाद और वैश्विक साहित्य का प्रभाव
- भारतीय भाषाओं के साहित्य का अंग्रेज़ी और अन्य भाषाओं में अनुवाद बढ़ा है, जिससे क्षेत्रीय साहित्य को पहचान मिल रही है।
- विदेशी लेखकों की किताबें भारतीय पाठकों के लिए ज्यादा सुलभ हो गई हैं।
स्वतंत्र लेखकों (Self-publishing) का उदय
- Amazon Kindle Direct Publishing और अन्य प्लेटफ़ॉर्म्स के माध्यम से लेखक अब खुद अपनी किताबें प्रकाशित कर सकते हैं।
- पारंपरिक प्रकाशकों पर निर्भरता कम हुई है।
(B) प्रमुख साहित्यिक विधाएँ
उपन्यास और लघुकथा – समकालीन जीवन, फेमिनिज़्म, जाति-वर्ग संघर्ष, डिजिटल जीवनशैली पर केंद्रित हैं।
कविता – मुक्त छंद कविता और हिंदी, उर्दू, पंजाबी, मराठी जैसी भाषाओं में नई लय और प्रयोगधर्मिता देखी जा रही है।
वेब-सीरीज़ आधारित लेखन – कई वेब-सीरीज़ साहित्यिक कृतियों पर आधारित हैं (जैसे “Scam 1992”, “Sacred Games”)।
इक्कीसवीं सदी में कला
(A) आधुनिक कला के नए स्वरूप
डिजिटल आर्ट और NFT (Non-Fungible Tokens)
- पारंपरिक चित्रकला और मूर्तिकला के साथ डिजिटल आर्ट का युग आ गया है।
- NFT कला (ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल आर्ट) ने कलाकारों को सीधे वैश्विक बाज़ार से जोड़ दिया है।
- Beeple की डिजिटल पेंटिंग “Everydays: The First 5000 Days” $69 मिलियन में बिकी थी।
फिल्म और वेब-सीरीज़ में कला का समावेश
- सिनेमा और वेब-सीरीज़ अब सामाजिक यथार्थ, पौराणिक कथाएँ और कल्पनाशीलता को नई तकनीक के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं।
- “RRR”, “Kantara”, और “Tumbbad” जैसी फिल्मों ने लोककथाओं और विज़ुअल आर्ट का बेहतरीन संयोजन किया है।
परफॉर्मिंग आर्ट्स (नाट्य और संगीत)
- फ्यूजन संगीत (Indian classical + Electronic) और इंडिपेंडेंट म्यूजिक की लोकप्रियता बढ़ी है।
- स्ट्रीट आर्ट और ग्रैफिटी – शहरी कला (Murals, Graffiti) बड़े शहरों में आम हो गई है।
- फैशन और टेक्सटाइल आर्ट – पारंपरिक भारतीय कला को समकालीन फैशन में नए रूप में देखा जा सकता है।
(B) कला के नए माध्यम
इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया आर्टिस्ट – कलाकार अब गैलरी के बजाय सोशल मीडिया पर अपनी कला बेचते हैं।
वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी (VR & AR) – कला प्रदर्शनियों और डिज़ाइन में इनका उपयोग बढ़ रहा है।
इंटरैक्टिव और पब्लिक आर्ट – बड़े शहरों में 3D म्यूरल्स और लाइट इंस्टॉलेशन्स के माध्यम से कला आम जनता तक पहुंच रही है।
निष्कर्ष
इक्कीसवीं सदी का साहित्य और कला तकनीक, वैश्वीकरण और नए सामाजिक-राजनीतिक विचारों से गहराई से प्रभावित हो रहे हैं। डिजिटल माध्यमों के विकास ने इन्हें अधिक लोकतांत्रिक और सुलभ बना दिया है। साथ ही, पारंपरिक रूपों में भी नवाचार हो रहा है, जिससे साहित्य और कला की नई परिभाषाएँ उभर रही हैं।
(v) जनसंचार माध्यम: उत्तरदायित्व या व्यवसाय
भूमिका
जनसंचार माध्यम (Mass Media) समाज में सूचना, विचारों और मनोरंजन का प्रमुख स्रोत हैं। समाचार पत्र, टेलीविज़न, रेडियो, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म लोगों को जागरूक करने और लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन आज के दौर में मीडिया का एक बड़ा हिस्सा व्यावसायिक हितों से प्रेरित हो गया है, जिससे यह प्रश्न उठता है: क्या जनसंचार माध्यम अपने उत्तरदायित्व को निभा रहे हैं, या केवल व्यवसाय बनकर रह गए हैं?
जनसंचार माध्यम का उत्तरदायित्व
जनसंचार माध्यमों का मूल उद्देश्य सत्य, निष्पक्षता और जनहित की रक्षा करना है। इनका समाज के प्रति निम्नलिखित उत्तरदायित्व है:
(A) सूचना का निष्पक्ष प्रसार
जनता तक सही, संतुलित और प्रमाणित जानकारी पहुँचाना।
अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं से बचना।
(B) लोकतंत्र की रक्षा
सरकार और नीतियों की निष्पक्ष आलोचना कर जनता को सशक्त बनाना।
सत्ता के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और सामाजिक अन्याय को उजागर करना।
(C) सामाजिक सुधार और जागरूकता
सामाजिक मुद्दों (जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण) पर जनमत तैयार करना।
नारी सशक्तिकरण, दलित उत्थान और बाल अधिकारों पर प्रकाश डालना।
(D) आपदा और संकट में जिम्मेदारी
कोविड-19 जैसी महामारी के दौरान सही जानकारी देना।
प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध जैसी स्थितियों में जनता तक त्वरित सूचना पहुँचाना।
(E) सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों का संरक्षण
समाज की विविधता और सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देना।
भड़काऊ या असंवेदनशील सामग्री से बचना।
जनसंचार माध्यम: एक व्यवसाय के रूप में
वर्तमान समय में जनसंचार माध्यम केवल सूचना का स्रोत नहीं, बल्कि एक बड़ा उद्योग बन चुके हैं। इन पर कॉर्पोरेट हित, विज्ञापन, राजनीतिक प्रभाव और टीआरपी का दबाव बढ़ता जा रहा है।
लाभ पर आधारित मीडिया
विज्ञापन-आधारित मॉडल – मीडिया संस्थान विज्ञापन से लाभ कमाते हैं, जिससे कई बार खबरों की निष्पक्षता प्रभावित होती है।
टीआरपी की होड़ – टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में टीआरपी और व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए सनसनीखेज और पक्षपातपूर्ण खबरें दिखाई जाती हैं।
पेड न्यूज़ और प्रायोजित कंटेंट – कई बार राजनीतिक या कॉर्पोरेट संस्थाएं समाचारों को प्रभावित करती हैं।
(B) राजनीतिक दबाव
मीडिया हाउसेज़ का राजनीतिक झुकाव – कुछ मीडिया संस्थान विशेष राजनीतिक दलों या विचारधाराओं के समर्थन में खबरें प्रसारित करते हैं।
स्वतंत्र पत्रकारिता पर खतरा – निष्पक्ष पत्रकारों और स्वतंत्र मीडिया संस्थानों पर दबाव डाला जाता है।
(C) भ्रामक और फेक न्यूज़ का बढ़ना
सोशल मीडिया पर गलत सूचना का प्रसार – व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जैसी प्लेटफॉर्म पर बिना सत्यापन के खबरें वायरल होती हैं।
न्यूज़ चैनलों में भ्रामक डिबेट – वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए भावनात्मक और विवादास्पद विषयों को बढ़ावा दिया जाता है।
संतुलन कैसे बनाया जाए?
स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया को बढ़ावा दिया जाए।
असत्य समाचारों और पेड न्यूज़ पर सख्त नियंत्रण हो।
मीडिया को केवल मुनाफे का साधन नहीं, बल्कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बनाए रखा जाए।
जनता को भी जागरूक होकर जिम्मेदार मीडिया की पहचान करनी होगी।
निष्कर्ष
जनसंचार माध्यमों का प्राथमिक उत्तरदायित्व समाज को जागरूक और सूचित करना है, लेकिन आधुनिक समय में यह व्यवसायिक लाभ और राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं। मीडिया को व्यावसायिक हितों से ऊपर उठकर अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाने की आवश्यकता है, ताकि यह लोकतंत्र की असली ताकत बना रहे।
5. निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य प्रयोग इस प्रकार कीजिए कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए : 1x8=8
(i) घाट-घाट का पानी पीना :- बहुत अनुभवी होना
(ii) दाना-पानी उठना :- स्थान छोड़ना
(iii) देवता कूच कर जाना :- मर जाना / भयभीत हो जाना
(iv) पगड़ी उछालना :- अपमान करना
(v) उन्नीस पड़ना :- कम पड़ना/जब कोई व्यक्ति किसी तुलना में पीछे रह जाए
(vi) ताक पर रखना :- उपेक्षा करना
(vii) आँच न आने देना :- कष्ट न आने देना
(viii) चाँदी कटना :- अधिक लाभ होना
3. निम्नलिखित वाक्यों को सुधारकर लिखिए: 1x6=6
बीमारी का कारण यह था कि वहाँ की जलवायु मेरे अनुरूप नहीं थी।
बीमारी का कारण यह था कि वहाँ की जलवायु मेरे अनुकूल नहीं थी।
जयशंकर प्रसाद ने ‘कामायनी’ की रचना लिखी है।
जयशंकर प्रसाद ने ‘कामायनी’ की रचना की है।
मैं और मेरे मित्रों को स्कूल की क्रिकेट टीम में चुना गया है।
मुझे और मेरे मित्रों को स्कूल की क्रिकेट टीम में चुना गया है।
विकास खाना खाकर के चारपाई पर पसर गया।
विकास खाना खा कर चारपाई पर लेट गया।
उसका जैसा अक्लमंद लड़का ढूँढे से न मिलेगा।
उसके जैसा अक्लमंद लड़का ढूँढे से न मिलेगा।
आप क्या दोगे, उसके पास तो पहले से ही बहुत कुछ है।
आप क्या देंगे ? उसके पास तो पहले से ही बहुत कुछ है।
7. कोष्ठक में दिए गए निर्देश के अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए: 1x6=6
अध्यापक ने छात्र को अनुशासन भंग करने पर सज़ा दी। (संयुक्त वाक्य में बदलिए)
अध्यापक ने छात्र को सज़ा दी क्योंकि उसने अनुशासन भंग किया।
मैंने उसे बहुत समझाया पर वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। (सरल वाक्य में बदलिए)
मेरे समझाने के बाद भी वह अपनी जिद पर अड़ा रहा।
समय-सीमा समाप्त होने तक कोई टीम गोल नहीं कर पाई। (संयुक्त वाक्य में बदलिए)
समय-सीमा समाप्त हो गई परन्तु कोई टीम गोल नहीं कर पाई।
शमी या तो खुद आएगा या किसी को भेजेगा। (मिश्र वाक्य में बदलिए)
यदि शमी खुद नहीं आएगा, तो वह किसी को भेजेगा।
वह जानता है कि यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानेगा तो क्या होगा। (सरल वाक्य में बदलिए)
वह परिणाम जानता है जो तुम्हारी बात न मानने पर होगा ।
मैं आपसे आर्थिक सहायता की प्रार्थना करता हूँ। (मिश्र वाक्य में बदलिए)
मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे आर्थिक सहायता दें।
8. निम्नलिखित प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द लिखिए: 1⁄2x8=4
(i) जो कहा न जा सके – अकथनीय
(ii) जिसकी कामना पूरी हो गई हो – परितुष्ट
(iii) जिसकी सहायता करनेवाला कोई न हो- निस्सहाय
(iv) जो निगाह से परे हो- परोक्ष
(v) जिसे दूसरों से छिपाकर रखना आवश्यक हो- गोपनीय
(vi) जिसमें इस ओर से उस ओर की वस्तुएँ दिखाई देती हों – पारदर्शी
(vii) सामान्य या व्यापक नियम/चलन के विरुद्ध बात- अपवाद
(viii) किसी काम के लिए पहले ही दिया जाना- पूर्वभुगतान
9. शुद्ध वर्तनीवाले शब्दों को चुनकर लिखिए: 1/2x12=6
बज़ार – बाज़ार , रुपया- रुपया, साधू– साधु, चहारदिवारी– चहारदीवारी, सामिग्री- सामग्री, दुरवस्था- दुरवस्था, हथिनी – हथिनी , आध्यात्म- अध्यात्म, कठनाई- कठिनाई , मंत्रिपरिषद्- मंत्रिपरिषद , निरपराधी- निरपराधी, मांस-मांस, आँदोलन-आंदोलन, धनाड्य- धनाढ्य, सम्मुचय- समुच्चय, नवाब-नवाब, रविंद्र – रवीन्द्र , दुस्साध्य- दुस्साध्य, प्रतिद्वंदी- प्रतिद्वंद्वी, उपलक्ष- उपलक्ष्य, सामर्थ्य- सामर्थ्य, स्वस्थ्य- स्वास्थ्य, बुद्धवार-बुधवार, मट्ठा- मट्ठा अंतर्धान- अंतर्ध्यान, अंताक्षरी- अंत्याक्षरी, यथेष्ट- यथेष्ट, अभ्यस्थ- अभ्यस्त, व्यक्तिक- वैयक्तिक, उत्कट- उत्कटासन, कृतकृत्य- कृतकृत्य , प्राकृति- प्रकृति, जगत्गुरु- जगद्गुरु
10. निम्नलिखित शब्दों का संधि-विच्छेद कीजिए 1⁄2 x10 = 5
- स्वेच्छा – स्व + इच्छा ( व्यंजन संधि)
- ब्रह्मर्षि- ब्रह्म + ऋषि (गुण संधि अ, आ के साथ इ, ई का मेल होने पर ‘ए’; उ, ऊ का मेल होने पर ‘ओ’; तथा ऋ का मेल होने पर ‘अर्’ हो जाता है)
- तथैव- तथा + एव ( वृद्धि संधि)
- प्रत्युत्पन्न – प्रति + उत्पन्न (गुण सन्धि)
- सर्वेक्षण- सर्व + ईक्षण(गुण स्वर संधि)
- उल्लेख- ‘उत् + लेख’
- संचय- सम् + चय’
- पुरस्कार – पुर: + ‘कार’
- चतुष्कोण – चतुः + कोण
- अनायास- अनै + आस ( अयादि संधि)
11. निम्नलिखित से बननेवाले विशेषण शब्द लिखिए: 1⁄2 x12=6
पृथ्वी – पार्थिव
वसंत → वसंती (वसंत ऋतु से संबंधित)
परिष्कार → परिष्कृत (संशोधित या निखरा हुआ)
विश्व → वैश्विक (संपूर्ण विश्व से संबंधित)
सूर्य → सौर (सूर्य से जुड़ा हुआ)
कृपा → कृपालु, कृपामय (दयालु, अनुग्रह से भरा)
परिवर्तन → परिवर्तनीय (जिसमें बदलाव हो सके)
गान → गायनशील, गेय (गाने योग्य)
दमन → दमनकारी (दमन करने वाला)
विवेचन → विवेचनात्मक (विश्लेषण से संबंधित)
परस्पर → परस्परिक (एक-दूसरे से संबंधित)
यौवन → युवा, युवावस्था (युवा अवस्था से जुड़ा हुआ)
12. निम्नलिखित शब्दों में आए प्रत्यय लिखिए : 1⁄2 x8=4
दिशा → -आ (यह संज्ञा सूचक प्रत्यय है)
कटाई → -आई (क्रिया से संज्ञा बनाने वाला प्रत्यय)
धिक्कार → -आर (भाववाचक संज्ञा बनाने वाला प्रत्यय)
सुनार → -आर (व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग होने वाला प्रत्यय)
समझौता → -औता (क्रिया से संज्ञा बनाने वाला प्रत्यय)
दबाव → -आव (भाव या दशा दर्शाने वाला प्रत्यय)
गढ़ंत → -अंत (क्रिया से संज्ञा बनाने वाला प्रत्यय)
पाठक → -अक (कर्त्ता या करने वाले को दर्शाने वाला प्रत्यय)
© 2026 Civilstap Himachal Design & Development